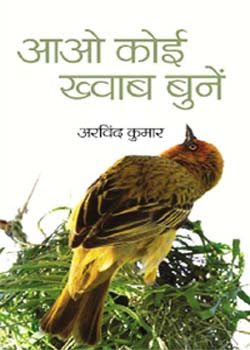|
| चित्र गूगल सर्च इंजन से साभार |
दिन हैं शर्मीले..
सिर पर चढ़ी धूप ने पहने
कपड़े कुहरीले
काँपें तन-मन चुभें शीत के
ये शर जहरीले।
चारों ओर धुंध का घेरा
नजर न कुछ आये
राख मले जोगी-सा मौसम
जिसे न जग भाये
दबे पाँव आकर छुप जाते
दिन हैं शर्मीले।
वृक्षों और लताओं के अब
पीत हुए पत्ते
इन पत्तों पर गिरे ओस-कण
आँसू-से झरते।
उपवन, खेत, मेड़, पगडण्डी
सब गीले-गीले।
पंछी दुबक गये कोटर में
सूनी अँगनाई
लेकिन चक्की से चूल्हे तक
नाच रही माई
सर्द अलाव हुआ तो बाबा
हुए लाल-पीले।
देहरी भीतर खुशियाँ आईं..
देहरी भीतर खुशियाँ आईं
लगता अपने दिन बहुरे हैं
बहुत दिनों के बाद हमारे
आँगन में पंछी उतरे हैं ।
अच्छी फसल हुई है अबकी
खूब हुए हैं चना औ' मटर
कुठला भरा हुआ गेहूँ से
धरे बरोठे राई-अरहर
बेच अनाज चुकाया कर्जा
ईश-कृपा से अब उबरे हैं ।
कजरारे नयना शर्मीले
दर्पण से खुलकर बतियाते
सेंदुर ,टिकुली और महावर
बिन बोले सब कुछ कह जाते
वर्षों बाद बज रही पायल
मेंहदी रचे हाथ निखरे हैं ।
शुभ-शुभ शगुन हो रहें हैं नित
कागा भी मुँडेर पर बोले
चैता,बन्ना गावै तिरिया
भेद जिया के रह-रह खोले
गेरू मिले हुए गोबर से
घर औ' द्वार लिपे संवरे हैं।
पिछले साल पड़ा सूखा तो
रोई मुनिया की महतारी
देवी की किरपा से अबकी
गौना देने की तैयारी
जो सम्बन्धी तने -तने थे
लगे तनिक वो भी निहुरे हैं।
आने वाली पीढी को हम..
आने वाली पीढी को हम
आओ सुखद जवानी दे दें
अपने जले पांव हों चाहे
उन को शाम सुहानी दे दें।
जहरीली जो हुईं हवाएं
उनमें भी वे जहर न भर दें
बढें कदम तो झंझाऐं आ
उंहें कहीं भयभीत न कर दें
डरें न झुकें उंहें हम ऐसा
गैरत वाला पानी दे दें।
नये दौर की चाल तेज है
आओ बढकर उन्हें सराहें
करवट बदल रहा है मौसम
बदल रही हैं उनकी चाहें
वे पिज्जा. बर्गर खाएं पर
थोडी .सी गुडधानी दे दें
वे अतीत के पृष्ठ सुनहरे
जिंहें भुलाना कभी न संभव
आने वाले कल की खातिर
फिर उनमें रंग भर दें अभिनव
पुरखों के स्वरणिम अतीत की
ताजा लिखी कहानी दे दें।
चाँद-सितारे छू कर भी हम..
चाँद-सितारे छू कर भी हम
मन से अभी आदिवासी हैं ।
घिरे हुए मोहक घेरों से
जिनके रंग-बिरंगे फंदे
इन फंदों में सभी फंसे हैं
मूरख,ज्ञानी,ध्यानी बन्दे
मुख्य पृष्ठ पर अभी जमे हैं
जो सन्दर्भ हुये बासी हैं।
तन्त्र-मन्त्र के जाल बिछे हैं
स्वांग सरीखे जादू टोने
दिशाशूल ,अपशगुन से डरें
माथे-माथे लगे दिठौने
जब हम तिलक भभूत लगायें
शिर धुनते मगहर-काशी हैं ।
भूमण्डलीकरण की बातें
लेकिन मन में बसे कबीले
सब पर गहरे रंग चढ़े हैं
लाल, हरे औ'नीले ,पीले
अणु बम सिर पर लादे फिरते
पर खुशियों के अभिलाषी हैं।
जाने कितने दर्पण बदले
लेकिन खुद को बदल न पाये
गहन अँधेरे मिटें न मेटे
कहने को हैं दीप जलाये
भयवश पलकें बन्द न होतीं
सुख के सपने अनिवासी हैं ।
अम्मा का मन कुढ़ता है..
फोटो वही पुरानी लेकिन
फ्रेम नया मढ़ना पड़ता है।
लोटा,थाली और कटोरों
का जारी है पीछे हटना
कब्जाए क्राकरी किचन को
ठप्पा जिस पर मेड-चाइना
बच्चों की खुशियों में खुश हूँ
पर अम्मा मन कुढ़ता है ।
ह्रदय-पटल पर खिंची रेख वो
कभी-कभी गहरी हो जाती
मोबाइल ,कम्प्यूटर हैं पर
मन फिर पढ़ना चाहे पाती
वे अतीत के पृष्ठ सुनहरे
अन्तस् व्याकुल हो पढ़ता है।
यादें बढ़ कर छाया देतीं
जब-जब तपने लगे दुपहरी
उन्हें भूलना बहुत कठिन है
ऐसी छाप पड़ी है गहरी
बीता कल सिर सहला देता
और कभी चांटा जड़ता है ।
नये चलन का है प्रभाव पर
रखता हूँ मैं खुद संयत
अभी संभाले हूँ वैसे ही
पुरखों से जो मिली विरासत
सुधियाँ उधर-उधर जातीँ,मन-
पंछी जिधर-जिधर उड़ता है।
तोड़ लो अनुबन्ध..
तोड़ लो अनुबन्ध जहरीली हवा से,
मन महासागर समय बहती नदी है ।
एक मन्थन ने प्रलय को रच दिया था
बस सुधा घट के लिए छल-किया था
कौन पीता विष भला सञ्जीवनी-सा
शंभु ने जिसको विहंस कर पी लिया था।
चेतना के सप्त स्वर बेचैन लगते
गरल है हर होंठ पर क्या त्रासदी है।
जाल फैलाये शिकारी मौन साधे
देखते चुपचाप बगुलों से इरादे
स्वर्ण-पिंजरे में सही पर कैद हैं हम
गत हुए हैं स्वप्न देखे एक-आधे
काट दो इन बंधनों की मेखला को
पीठ पर वैताल बन कर जो लदी है।
सिमट आये हैं छितिज घर -आंगनों में
दर्द के अहसास जगते फागुनों में
बाँसुरी क्यों मोहिनी लगती नहीं अब
हाट के पर्याय हैं वृंदावनों में
बन्द नैनों से नहीं दर्पण निहारो
नव किरण ले चल रही नूतन सदी है।
छुट्टी पर है घाम (दोहे)
कुहरे ने फिर खत लिखा
है सूरज के नाम
अब ड्यूटी पर मैं डटा
छुट्टी पर है घाम।
ठण्ड ओस से घास पर
सजा रही बाजार
औ' बढ़ता ही जा रहा
कुहरे का व्यापार।
ठिठुरन बढ़ती जा रही
ज्यों- ज्यों बढ़ती शीत
ठंडक का दिखता असर
पात हुये हैं पीत।
कुहरे का ऐसा असर
मौसम साधे योग
पंछी कोटर में छुपे
सिकुड़े-सिमटे लोग ।
मौसम वैरागी हुआ
मले वदन में राख
माघ-पूस कुहरा ढँके
घटी सूर्य की साख ।
सर्दी से बेहाल सब
मांगें रब से खैर
सूरज भी लगता डरा
भुला दिया है बैर ।
छाया कुहरा छँट गया
जो था बड़ा अरूप
कल तक ठिठुरी थी बहुत
आज खिली है धूप ।
देवेन्द्र सफल
- पूरा नाम-देवेन्द्र कुमार शुक्ल
- पिता- कीर्तिशेष लक्षमी नारायण शुक्ल
- माता- समृतिशेष अलक नंदा देवी शुक्ला
- जन्म-स्थान-कानपुर महानगर (उ.प्र)
- जन्म तिथि-04-01-1958
- शिक्षा-स्नातक
- प्रकाशन-गीत-नवगीत संग्रह: पखेरू गन्ध के, नवांतर, लेख लिखे माटी ने, सहमी हुई सदी, हरापन बाक़ी है।
- अन्य अनेक सामूहिक संकलनों में रचनाएँ प्रकाशित।
- प्रसारण-आकाशवाणी के मान्य कवि ।
- सम्मान-देश-विदेश में अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित/ पुरस्कृत।
- संपर्क-117/क्यू / 759 -ए,शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208025
- ईमेल-devendrasafal@gmail.com